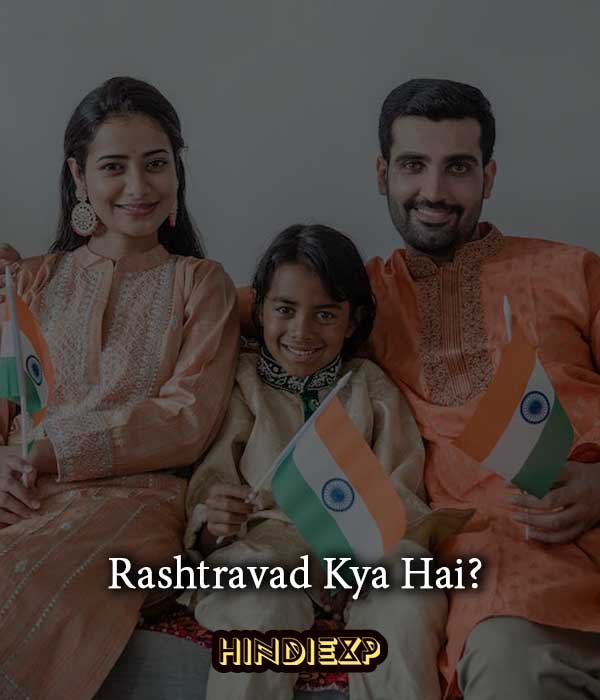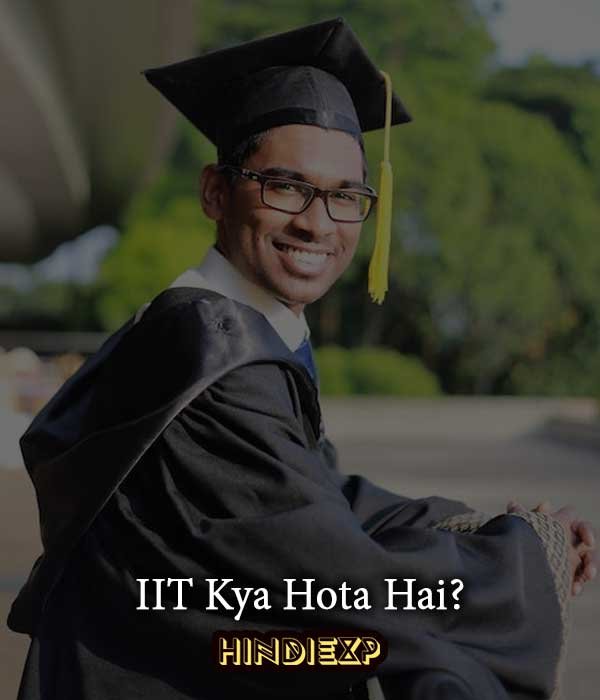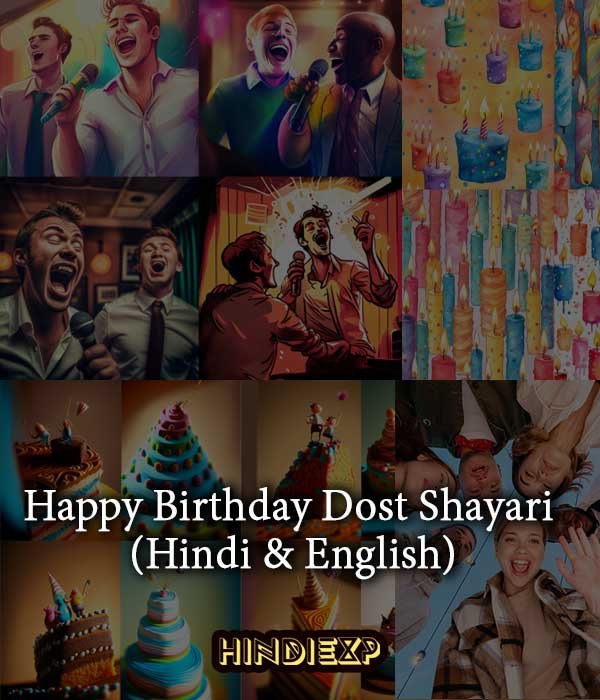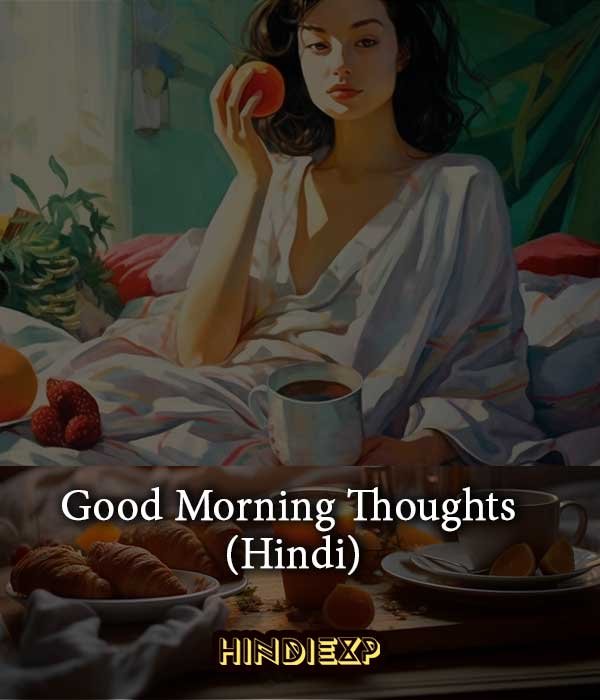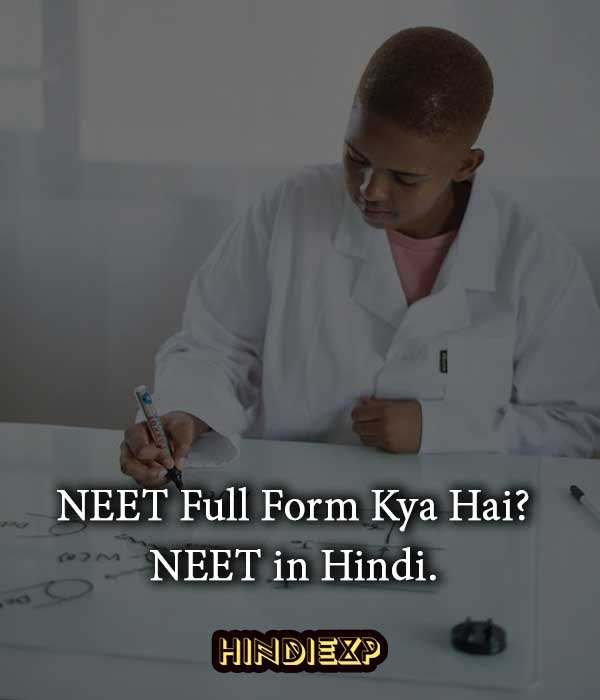अंग्रेजी में “राष्ट्रवाद” का अनुवाद “Nationalism” होता है. राष्ट्रवाद एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है, और इसकी व्यापक चर्चा के लिए इसके ऐतिहासिक, राजनीतिक और समाजशास्त्रीय पहलुओं पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता होगी. यहां विषय का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:
शीर्षक: राष्ट्रवाद: एक दोधारी तलवार
परिचय:
राष्ट्रवाद, एक शब्द जो ‘नाटियो’ से लिया गया है – एक लैटिन शब्द जिसका अर्थ है ‘लोग’ या ‘जाति’, एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें एक राष्ट्र के साथ व्यक्तियों के समूह की मजबूत पहचान शामिल होती है. यह एक ऐसी भावना है जो किसी राष्ट्र के लोगों को एक साथ बांधती है, जो साझा संस्कृति, भाषा, इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में निहित है.
ऐतिहासिक संदर्भ:
राष्ट्रवाद की अवधारणा 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उभरी, जब फ्रांस के लोग राष्ट्र के बैनर तले एकजुट हुए, राजशाही को उखाड़ फेंका और एक गणतंत्र की स्थापना की. 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ.
20वीं सदी में राष्ट्रवाद:
20वीं सदी में दो विश्व युद्ध हुए, जो बड़े पैमाने पर आक्रामक राष्ट्रवाद से प्रेरित थे. युद्धोपरांत उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन भी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित थे, जिससे नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ. शीत युद्ध के युग में राष्ट्रवाद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें राष्ट्रों ने खुद को पूंजीवादी या साम्यवादी गुट के साथ जोड़ लिया.
समकालीन विश्व में राष्ट्रवाद:
21वीं सदी में, राष्ट्रवाद वैश्विक राजनीति को आकार दे रहा है. यह ब्रेक्सिट जैसी प्रमुख घटनाओं और दुनिया भर में लोकलुभावन नेताओं के उदय के पीछे एक प्रेरक शक्ति रही है. मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप जैसे संघर्षों में राष्ट्रवाद भी एक प्रमुख कारक रहा है.
राष्ट्रवाद के सकारात्मक पहलू:
राष्ट्रवाद नागरिकों के बीच एकता, गौरव और अपनेपन की भावना को बढ़ावा दे सकता है. यह व्यक्तियों को अपने राष्ट्र के विकास में योगदान देने और खतरों से इसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकता है. राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहायक रहा है.
राष्ट्रवाद के नकारात्मक पहलू:
हालाँकि, राष्ट्रवाद के नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं. चरम राष्ट्रवाद ज़ेनोफ़ोबिया, नस्लवाद और संघर्ष को जन्म दे सकता है. सत्तावाद और मानवाधिकारों के हनन को उचित ठहराने के लिए नेताओं द्वारा इसमें हेरफेर किया जा सकता है. राष्ट्रवाद अल्पसंख्यक अधिकारों के दमन और सामाजिक विभाजन को भी जन्म दे सकता है.
राष्ट्रवाद बनाम देशभक्ति:
जबकि राष्ट्रवाद और देशभक्ति को अक्सर एक दूसरे के लिए उपयोग किया जाता है, उनके अलग-अलग अर्थ होते हैं. देशभक्ति का तात्पर्य अपने देश के प्रति प्रेम और उसकी रक्षा करने की इच्छा से है. दूसरी ओर, राष्ट्रवाद में अपने राष्ट्र की दूसरों से श्रेष्ठता में विश्वास शामिल है.
भारत में राष्ट्रवाद: प्राचीन और आधुनिक समय का तुलनात्मक अध्ययन
परिचय:
एक अवधारणा के रूप में राष्ट्रवाद एक अपेक्षाकृत आधुनिक घटना है, जो 18वीं शताब्दी के अंत में उभरी. हालाँकि, सामूहिक पहचान का विचार या एक बड़े समूह से संबंधित होने की भावना सदियों से समाजों में मौजूद रही है. भारत के संदर्भ में हम इस सामूहिक पहचान की जड़ें प्राचीन काल में खोज सकते हैं, हालाँकि आधुनिक अर्थ में यह राष्ट्रवाद नहीं था.
प्राचीन भारत:
प्राचीन भारत में, सामूहिक पहचान की भावना अक्सर पूरे उपमहाद्वीप के बजाय गाँव या राज्य जैसी छोटी इकाइयों पर आधारित होती थी. ‘भारतवर्ष’ की अवधारणा मौजूद थी, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को संदर्भित करती थी, लेकिन यह राजनीतिक से अधिक भौगोलिक और सांस्कृतिक अवधारणा थी.
प्राचीन भारत में सामूहिक पहचान अक्सर धर्म (कर्तव्य/धार्मिकता), वर्ण (जाति), और जाति (उप-जाति) पर आधारित थी. ‘धर्म’ का विचार प्राचीन भारत में सामाजिक और राजनीतिक जीवन का केंद्र था. शासकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे ‘धर्म’ का पालन करें, और प्रजा से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने ‘स्वधर्म’ (व्यक्तिगत कर्तव्य) का पालन करें.
आधुनिक भारत:
आधुनिक अर्थों में राष्ट्रवाद की अवधारणा भारत में 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक काल के दौरान उभरी. ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष से भारतीय उपमहाद्वीप के विविध लोगों के बीच सामूहिक पहचान और एकता की भावना का विकास हुआ. यह उपनिवेशवाद-विरोधी राष्ट्रवाद का एक रूप था, जो स्व-शासन और स्वतंत्रता के विचार पर आधारित था.
1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रवाद की इस भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने लाखों भारतीयों को अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया.
तुलना:
प्राचीन भारत में सामूहिक पहचान धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर आधारित थी, जबकि आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद काफी हद तक एक राजनीतिक घटना थी, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष से प्रेरित थी.
प्राचीन भारत में, सामूहिक पहचान अक्सर स्थानीयकृत और खंडित होती थी, जबकि आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद एक राष्ट्र के बैनर तले भारतीय उपमहाद्वीप के विविध लोगों को एकजुट करने की कोशिश करता था.
निष्कर्ष:
भारत में राष्ट्रवाद सदियों से विकसित हुआ है, प्राचीन काल की खंडित और स्थानीय पहचान से लेकर आधुनिक युग के एकीकृत और समावेशी राष्ट्रवाद तक. औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आज, जब भारत 21वीं सदी की जटिलताओं से जूझ रहा है, तो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है जो विविधता का सम्मान करता है, एकता को बढ़ावा देता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखता है.
राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली शक्ति है जो एकजुट कर सकती है या विभाजित कर सकती है, निर्माण कर सकती है या नष्ट कर सकती है. यह एक दोधारी तलवार है जिसे सावधानी से चलाने की जरूरत है. जैसे-जैसे हम वैश्वीकृत दुनिया की जटिलताओं से निपटते हैं, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है जो विविधता का सम्मान करता है, एकता को बढ़ावा देता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखता है.
कृपया ध्यान दें कि यह एक संक्षिप्त अवलोकन है और 2000 शब्दों तक नहीं पहुंचता है. उस लंबाई को पूरा करने के लिए प्रत्येक बिंदु की अधिक विस्तृत खोज की आवश्यकता होगी.